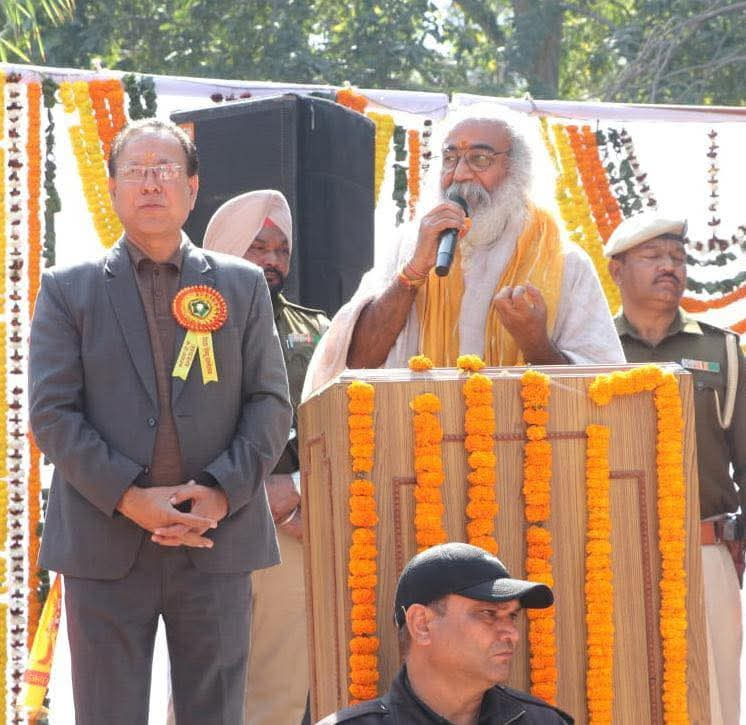डा. हरीश चंद्र लखेड़ा
बरसात का यह मौसम उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू-कश्मीर और पंजाब के लिए एक अभिशाप बनकर आया। कहीं बादल फटे, कहीं उफनती नदियां गांवों, कस्बों और खेतों को निगल गईं, तो कहीं पहाड़ों से टूटकर आए मलबे ने बस्तियां मिटा दीं। अधिकतर सड़कें भी टूट गईं। मोटे तौर पर अब तक 800 पार कर चुका है। इनमें से अधिकतर लोग या तो मारे गए या लापता हैं। हज़ारों पशु बाढ़ की गाद में समा गए। ये आंकड़े 30 अगस्त 2025 तक की खबरों पर आधारित हैं। स्थिति बदल सकती है क्योंकि बचाव और राहत कार्य चल रहे हैं। हर संख्या के पीछे एक टूटा हुआ परिवार, उजड़ा हुआ घर और बुझी हुई उम्मीदें छिपी हैं। सवाल यह है कि क्या यह केवल प्रकृति का प्रकोप था, या हमारी नीतियों की लापरवाही, अनियंत्रित निर्माण और चेतावनियों की अनसुनी का नतीजा? इस त्रासदी की असली जिम्मेदार कौन है?
इस साल 2025 का मानसून उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों के लिए काल साबित हुआ है। जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बादल फटने, भूस्खलन और उफनती नदियों ने भारी तबाही मचाई है। सैकड़ों गांव उजड़ गए, हजारों परिवार बेघर हो गए और खेत-खलिहान बर्बाद हो गए।
उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, उत्तराखंड में अब तक 75 से 80 लोगों की मौत हो चुकी है और 90 से 100 लोग लापता हैं। उत्तरकाशी के धराली गांव की त्रासदी में अकेले 100 से अधिक लोग लापता हुए। रुद्रप्रयाग, चमोली और टिहरी जिलों में भी कई घर उजड़ गए।
हिमाचल प्रदेश सबसे ज्यादा प्रभावित रहा। यहां 355 से 406 मौतें दर्ज हुई हैं और 40 से 49 लोग अब भी लापता हैं। मंडी, कांगड़ा, शिमला और चंबा जिलों में सबसे ज्यादा तबाही देखने को मिली। हजारों मकान ढह गए और करीब 1,800 से अधिक पशु बह गए।
जम्मू-कश्मीर में 130 से 150 लोग मारे गए हैं और 33 से 50 लोग लापता बताए जा रहे हैं। किश्तवाड़ के चिशोती गाँव में बादल फटने से अकेले साठ से अधिक लोगों की मौत हो गई। वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर भूस्खलन में भी दर्जनों श्रद्धालु मारे गए।
इन तीनों राज्यों को मिलाकर कुल मौतों का आंकड़ा 500 पार कर चुका है, जबकि लापता लोगों की संख्या 300 से अधिक बताई जा रही है। यानी अब तक 800 से अधिक लोग या तो मारे जा चुके हैं या लापता हैं।
ये आंकड़े केवल संख्या नहीं हैं, बल्कि हर एक आंकड़ा एक टूटा हुआ परिवार, एक उजड़ा हुआ गांव और एक बुझा हुआ सपना है। पहाड़ों में हर साल दोहराई जाने वाली यह त्रासदी अब केवल प्रकृति का कोप नहीं, बल्कि हमारी नीतियों की लापरवाही और अनियंत्रित विकास का भी परिणाम लगती है। सवाल यही है कि इस विनाश का असली जिम्मेदार आखिर कौन है—प्रकृति या हम खुद?
हिमालय केवल भारत का जल मीनार ही नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था और जीवन का आधार भी है। लेकिन हर साल यहां मानसून के साथ आने वाली आपदाएं यह सवाल उठाती हैं कि आखिर हिमालयी राज्यों की बारिश की आपदा के लिए कौन जिम्मेदार है। कौन हर साल सैकड़ों लोगों के मारे जाने या गायब होने के लिए जिम्मेदार है, कौन हजारों पशुओं की मौत का जिम्मेदार है? योजना आयोग की 40 साल पहले की एस. जेड. काज़िम की रिपोर्ट की उपेक्षा किसने की? क्यों हिमालयी विकास प्राधिकरण नहीं बन पाया? क्यों हिमालयी फंड अधर में लटका रहा और क्यों पर्यटन के नाम पर हिमालय में अनियंत्रित भीड़ भेजी जा रही है। इन सवालों के जवाब केवल प्राकृतिक आपदा तक सीमित नहीं, बल्कि नीति, शासन और विकास के मॉडल में छिपे हैं।
इस साल 6 अगस्त 2025 को उत्तरकाशी के धराली गांव में अचानक आई बाढ़ ने पलभर में गांव का बड़ा हिस्सा बहा दिया। पाच लोगों की मौत हुई, सौ से अधिक लोग लापता हुए और सैकड़ों पशु बह गए। यह कोई पहली घटना नहीं थी। 2013 की केदारनाथ आपदा, 2021 की चमोली-रैणी त्रासदी, 2023 में हिमाचल और सिक्किम की विनाशकारी बाढ़-भूस्खलन और अब 2025 की धराली त्रासदी—ये सभी उदाहरण बताते हैं कि हिमालय अब आपदा प्रयोगशाला बन चुका है।
यह बताना ्रावश्यक है कि 1982 में योजना आयोग ने हिमालयी क्षेत्र के सतत विकास के लिए एक उप-समूह बनाया था, जिसकी अध्यक्षता एस. जेड. काज़िम ने की। काजिम कमेटी की रिपोर्ट ने हिमालय में भविष्य में आने वाले खतरों की ओर इशारा किया था और ठोस समाधान सुझाए थे। इसमें हिमालयन विकास बोर्ड बनाने, हिमालयन फंड तैयार करने, नदियों और झरनों की डिजिटल मैपिंग करने, फ्लड प्लेन में निर्माण रोकने, स्थानीय समुदायों को प्राथमिक अधिकार देने और विशेष आपदा प्रबंधन व अनुसंधान संस्थान स्थापित करने की सिफारिश की गई थी। लेकिन इन सिफारिशों को या तो ठंडे बस्ते में डाल दिया गया या आधे-अधूरे तरीके से लागू किया गया।
इधर, उत्तराखंड ही नहीं, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर से लेकर सिक्किम तक में पिछले तीन दशकों में हिमालय में कई बड़ी आपदाएं आईं। 1998 में पिथौरागढ़ के मालपा गांव का विनाश, 2003 में उत्तरकाशी भटवाड़ी की त्रासदी, 2010 में लेह में बादल फटना, 2013 का केदारनाथ हादसा, जिसमें पांच हजार से अधिक लोग मारे गए, 2021 की रैणी-चमोली आपदा, 2023 में हिमाचल की तबाही और सिक्किम की तीस्ता घाटी उजड़ना और अब धराली का हादसा से लेकर जम्मू व हिमाचल की ये सभी घटनाएं बताती हैं कि यह केवल प्राकृतिक आपदाएँ नहीं बल्कि मानवीय लापरवाही से बढ़ी त्रासदियाँ हैं।
इन आपदाओं के लिए सबसे बड़ा कारण सरकारी उदासीनता है। काज़िम रिपोर्ट की सिफारिशें 40 साल से लागू नहीं हो पाईं। होटल, हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट और सड़कें नदी किनारों और फ्लड प्लेन में बनाई गईं। चारधाम यात्रा और ट्रैकिंग के नाम पर लाखों पर्यटकों की अनियंत्रित भीड़ भेजी जाती है। नीति आयोग और राज्यों की कमजोर भूमिका के कारण 2017 में बनी हिमालयन स्टेट रीजनल काउंसिल और 2018 का हिमालयन प्राधिकरण कागजों तक सीमित रह गए। आपदा प्रबंधन और अनुसंधान संस्थान का अभाव है।
पर्यटन के नाम पर भीड़ बढ़ाने की प्रवृत्ति भी खतरनाक है। इस तीन राज्यों में हर साल सात-आठ करोड़ लोग पहुंच रहे हैं। लाखों वाहन भी। हिमालयी राज्य पर्यटन से राजस्व कमाना चाहते हैं लेकिन वे कैरीइंग कैपेसिटी की परवाह किए बिना अंधाधुंध भीड़ खींच रहे हैं। केदारनाथ यात्रा में हर साल लाखों लोग सीमित इलाके में भेजे जाते हैं, धराली जैसे छोटे गांवो में होटल और होम-स्टे की भरमार है जिससे नदियों का प्राकृतिक प्रवाह बाधित होता है और सड़क चौड़ीकरण परियोजनाएं पहाड़ों को अस्थिर बना रही हैं। पहाड़ में बड़े-बड़े बांध कहीं बादल फटने की घटनाओं के लिए जिम्मेदार तो नहीं हैं? या पहाड़ों में उड़ते हेलीकाप्टर? सरकार को इसका अध्ययन कराना चाहिए।
एक बात यह भी कि हिमालयी विकास प्राधिकरण और फंड अधर में हैं क्योंकि केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय की कमी है। राजस्व और ठेकेदारों के दबाव में पर्यावरणीय अनुशासन की अनदेखी की जाती है। नीतियाँ अल्पदृष्टि राजनीति की भेंट चढ़ जाती हैं। परिणामस्वरूप न तो हिमालयी विकास बोर्ड बन पाया, न ही फंड का उपयोग सतत विकास के लिए हो सका।
धराली जैसी त्रासदियों से बचने के लिए अब केवल राहत और मुआवज़ा काफी नहीं है। हिमालयी विकास प्राधिकरण का गठन करना होगा, हिमालयन फंड का पुनर्गठन और पारदर्शी उपयोग सुनिश्चित करना होगा, नदियों और ग्लेशियरों की डिजिटल मैपिंग करनी होगी, फ्लड प्लेन में निर्माण पर सख्त रोक लगानी होगी, स्थानीय समुदायों को प्राथमिक अधिकार देने होंगे और हिमालयन आपदा अनुसंधान संस्थान की तत्काल स्थापना करनी होगी।
धराली की खीर गंगा त्रासदी समेत इस बार की आपदाएं केवल एक प्राकृतिक घटना नहीं, बल्कि नीति विफलता, लालफीताशाही और अल्पदृष्टि विकास मॉडल का परिणाम है। यदि चार दशक पहले दी गई एस. जेड. काज़िम रिपोर्ट की सिफारिशों को लागू किया गया होता तो शायद सैकड़ों जानें बचाई जा सकती थीं। आज फिर सवाल वही है—हिमालयी राज्यों की बारिश की आपदा के लिए कौन जिम्मेदार है। जब तक इस सवाल का ईमानदारी से जवाब नहीं दिया जाता और ठोस कदम नहीं उठाए जाते, तब तक हिमालय हर साल हमें और डरावनी चेतावनियां देता रहेगा। इसलिए भारत के नीति निर्धारकों को हिमालय की सुध ले लेनी चाहिए।